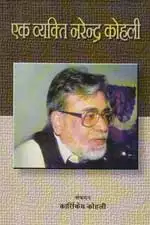|
संस्मरण >> एक व्यक्तित्व नरेन्द्र कोहली एक व्यक्तित्व नरेन्द्र कोहलीकार्तिकेय कोहली
|
443 पाठक हैं |
|||||||
नरेन्द्र कोहली के व्यक्तित्व से पहचान कराते संस्मरण...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
किसी लेखक के कृतित्व को उसकी रचनाएं पढ़कर जाना जा सकता है किंतु उसके
व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके निकट रहना आवश्यक है। उसके साथ समय
बिताना होता है। पापा के साथ हमारे जिन परिजनों, मित्रों तथा संबंधियों ने
समय बिताया है, उनकी उनके विषय में अनेक प्रकार की दृढ़बद्ध धारणाएं हैं।
आवश्यक नहीं कि वे सब लोग परस्पर सहमत ही हों। उनके मतभेद पापा के
व्यक्तित्व के कुछ नए कोण उभारते हैं। परिवार में जो बड़े हैं, उन्होंने
पापा को विकसित होते देखा है। समवयस्कों ने उनके साथ चलकर उनको परखा है।
अवस्था में छोटे लोगों ने केवल उनकी गुरुता को ही जाना है। पर सबसे अधिक
तो पापा ने अपने आपको देखा है। इसीलिए हमने इस पुस्तक में दो प्रकार के
संस्मरणों को संकलित किया है। पहले खंड में पापा को दूसरों की दृष्टि से
देखा गया है और दूसरे खंड में पापा ने स्वयं अपने-आपको देखा है। बहुत संभव
है कि उनको जाननेवाले किसी व्यक्ति को लगे कि ये सारे संस्मरण मिलकर भी
पापा के व्यक्तित्व को पूर्णता से प्रस्तुत नहीं करते। यह सत्य ही है,
क्योंकि किसी सर्जक के मनन, चिंतन, भावना, आकांक्षा और साधना को कुछ
निबंधों और संस्मरणों में पूर्णता से तो नहीं बांधा जा सकता। फिर भी मेरा
विचार है कि इन संस्मरणों में प्राय: वे सारे आयाम अपनी झलक दिखा ही देते
हैं, जिनके विषय में पाठक और शोधार्थी जानने को सदा उत्सुक रहते हैं। यह
पुस्तक हमारी ओर से पापा की षष्टिपूर्ति पर उनके लिए एक छोटी-सी भेंट है।
कार्त्तिकेय कोहली
खंड-एक
वदंति
नरेन्द्र कोहली : जनवादी से अध्यात्मवादी तक
डॉ.विवेकी राय
कथाकार नरेन्द्र कोहली से मेरा परिचय उनकी कृतियों के माध्यम से हुआ। उनकी
आरंभिक कृतियों में से ‘आश्रितों का विद्रोह’ और
‘आतंक’ ने ध्यान आकर्षित किया था; परन्तु
‘साथ सहा गया दुख’ नामक कृति ने इतना प्रभावित किया
कि कृतिकार को बधाई दिए बिना नहीं रह सका। यहीं से पत्र-व्यवहार आरंभ हुआ
और वह चलता गया। उन दिनों मेरी आदत थी कि जो पुस्तक पढ़ने में अत्यधिक
आकर्षित करती थी और जिस के वस्तु और शिल्प, दोनों पक्ष की समृद्धि मन को
छूने लगती थी, उस पर मैं लिखने बैठ जाया करता था। यह लिखना अथवा
समीक्षा-कर्म प्राय: समीक्षा के लिए नहीं, लेखक के सृजन-सौंदर्य को
आत्मसात् करने के लिए होता था।
‘साथ सहा गया दुख’ (सन् 1974 ई.) पर भी मैंने लिखा। यह देख कर मुझे आश्चर्य होता था कि मात्र ढाई पात्रों (पति, पत्नी और एक नवजात बच्ची) का सादा सपाट घरेलू या पारिवारिक उपन्यास इतना आकर्षक और गतिवान कैसे बन गया है। अनलंकृत जीवन-भाषा में सादगी का सौंदर्य घोल कर किस कला से इसे इतनी सघन संवेदनीयता से पूर्ण बनाया गया है। बाद में मालूम हुआ कि पहली बच्ची के जन्म और मृत्यु की यह जो कथा सन् 1966-67 ई. में लिखी गई, उसमें कल्पना बहुत कम है। जो है, वह लेखक का अनुभव है, भोगा हुआ सत्य है। इतने पर भी उस भुक्त दु:ख-सत्य को पारिवारिक जीवन-मूल्यों के शिव से संपृक्त कर, रचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत कर देने वाले शिल्प-सौंदर्य का सवाल तो लेखक की ओर आकर्षित कर ही देता है।
यह आकर्षण सन् 1975 ई. से और अधिक बढ़ गया। उनकी रामकथा वाली श्रृंखला की पहली कृति ‘दीक्षा’ इसी समय छपी थी। इसमें परंपरित अवधारणाओं पर जो नई प्रगतिशील जनवादी कलम लगाई गई थी, उसने कृति को जोरदार चर्चा का विषय बना दिया। एक प्रश्न उठा कि श्रद्धा, भावुकता और पूज्य-भाव की अतिमानवीय कल्पनाओं को बुद्धिवादी कैंची से कतर डालना और पौराणिक अथवा सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक राजनीतिक व्याख्या प्रस्तुत करना कहां तक उचित है ? इसका उत्तर नरेन्द्र कोहली ने ‘दीक्षा’ की भूमिका में देने का प्रयत्न किया है। बांगलादेश में क्रूर पाकिस्तानी सेनाओं के बर्बर अत्याचार और बुद्धिजीवियों के व्यापक संहार को देख कर उपन्यासकार के मन में रामकथा की नई व्याख्या उभर आती है और वह सोचता है, ‘‘बांगलादेश कहां है ? वह सिद्धाश्रम में भी हो सकता है।...पाकिस्तान तब नहीं था, किंतु राक्षस तो थे।...’’ इस प्रकार विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में तत्कालीन बुद्धिजीवियों की पीड़ाप्रसूत, राम के क्रांतिकारी नेतृत्व की यह नूतन गाथा उपन्यस्त होती है।
‘दीक्षा’ के बाद अगले वर्ष सन् 1976 ई. में रामकथा का दूसरा भाग ‘अवसर’ और इसी प्रकार प्रतिवर्ष उस श्रृंखला के एक-एक नए भाग के प्रकाशन-क्रम में सन् 1979 ई. तक शेष ‘संघर्ष की ओर’ और ‘युद्ध’ (दो भाग) का प्रकाशन संपन्न हो गया। वास्तव में यह बहुत श्रमसाध्य और महान् कार्य रहा। इसकी संपन्नता के साथ लेखक के रचनात्मक व्यक्तित्व की ऊंचाई बहुत बढ़ गई। ऐसे प्रिय लेखक से मिलना एक सुखद अनुभव था। मिलने का यह पहला मौका कलकत्ते में भारतीय संस्कृति संसद की ओर से आयोजित सन् 1983 ई. वाले कथा-समारोह में मिला। यह आयोजन 23 दिसंबर से शुरू होकर तीन दिनों तक रहा। इस में जैनेंद्र जी, निर्मल वर्मा, रामदरश मिश्र, भीष्म साहनी, अवध नारायण मुद्गल, राजी सेठ, उषा प्रियंवदा, गोविन्द मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, हिमांशु जोशी, बटरोही, सिद्धेश, प्रभाकर माचवे, चंद्रकांत बांदिवडेकर और नरेन्द्र कोहली आदि लेखकों ने भाग लिया था।
नरेन्द्र कोहली को इस समारोह में निकट से देखने का मौका मिला। वे कम बोलने वाले, गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति लगे। अपने भाषणों में वे समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से उठाते रहे। वे अपने को प्रस्तुत करने में बहुत सावधानी बरतते रहे। वे कभी बलपूर्वक स्थापित करने की चेष्टा नहीं करते थे। उनके विचारों में विस्तार-वृत्ति होती थी। इतने पर भी वे बोलने में अधिक समय नहीं लेते थे। उनका बोलना मौलिक चिंतन और आधुनिकता की चेतना से पूर्ण होता। उक्त सम्मेलन में अंतिम दिन 25 दिसंबर को अंतिम सत्र ‘मूल्य : मूल्यांकन : पुनर्मूल्यांकन’ के अंतर्गत डॉ.नरेन्द्र कोहली ने कहा, ‘‘जिस रचनाकार के पास कहने को अपनी बात है, वही काल-प्रवाह में टिक पाता है। यही कारण है कि प्रेमचंद का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, जबकि उग्र, चतुरसेन शास्त्री आदि अपने समय में बहुत चर्चित होने के बावजूद आज धूमिल होते जा रहे हैं।’’
उक्त कथन में ‘अपनी बात’ वाला तथ्य बहुत मूल्यवान है। नए बदलते समाज की नई चेतना और नई संवेदना तथा नई सोच को, ताजी ऊर्जा के साथ मौलिक शिल्प में प्रस्तुत करने वाले कथाकार नरेन्द्र कोहली के पास निर्विवाद रूप से कहने के लिए अपनी बात है। यहां तक कि वे वाल्मीकि और व्यास की बातों को उठाते हैं तो उसे प्रस्तुत करने में अपनी बात बना देते हैं और अविरोध, अनवरोध कह डालते हैं। अपने इसी नवाग्रही व्यक्तित्व के चलते ही वे अत्यंत जागरूकता के साथ जहां भी अवसर मिलता है, नएपन को अन्वेषित करते रहते हैं।
कलकत्ते के उक्त कथा-समारोह में यद्यपि पूरे दिन के कार्यक्रम बहुत कसावपूर्ण होते थे, तथापि रात में समय निकाल कर कोहली जी कलकत्ते की रंगकर्मी संस्थाओं को आधुनिकतम प्रस्तुतियों को बहुत रुचिपूर्वक देख आते थे। इस कार्य में मार्गदर्शक श्री विष्णुकांत शास्त्री हुआ करते थे। कलकत्ते के प्रयोगधर्मी नाटकों, उनको प्रस्तुत करने वाली विविध संस्थाओं, रंगमंचों तथा रंगशिल्पियों आदि में शास्त्री जी की बहुत गहरी पैठ थी। वे स्वयं उनके अटूट भाव से जुड़े थे और उनकी ओर से वे आगत कथाकारों को विधिवत् आमंत्रित करते थे। लोग जाते भी थे और रंगमंचविहीन तथा रंगसज्जा आदि रहित अनौपचारिक प्रस्तुतियों से प्रभावित भी होते थे। स्वयं आधुनिक दृष्टिसंपन्न कथाकार के साथ नाटककार होने के कारण नरेन्द्र कोहली इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। ‘शंबूक की हत्या’ निर्णय रुका हुआ, और ‘गारे की दीवार’—तीन नाट्य कृतियां, तब तक प्रकाशित हो चुकी थीं और किसी-न-किसी कोने से चर्चा आ जाती थीं।
दूसरी बार कुछ और अधिक निकट से परिचय का सुयोग एक स्वागत समारोह में हुआ। स्वागत मेरा ही हो रहा था। समारोह अखिल भारतीय लेखक संगठन, दिल्ली की ओर से डॉ.रामदरश मिश्र ने अपने आवास पर (17 फरवरी सन् 1987 ई.) आयोजित किया गया था। मैं उन दिनों उनका अतिथि था। पहली बार दिल्ली गया था। मेरा गंवार लेखक इस स्वागत से बहुत संकुचित हो रहा था। समारोह में कोहली जी के अतिरिक्त डॉ.कमलकिशोर गोयनका, डॉ.नरेन्द्र मोहन, डॉ.रमाकांत श्रीवास्तव, डॉ.ललित शुक्ल, डॉ.विजयेन्द्र स्नातक, और डॉ.विनय आदि साहित्यकार उपस्थित थे। डॉ.नरेन्द्र कोहली ने दिल्ली-संबंधी मेरे अनुभव के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उसे एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, ‘‘दिल्ली एक लड़ाई है।’’ और फिर अपनी यात्रा-भीरुता के परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या की। सचमुच डॉ.मिश्र के साथ दिल्ली में लगभग एक सप्ताह तक घूमने में मुझे ऐसा ही लगा था। कहीं भी जाना, बसों की भारी भीड़ में धंसना मेरे लिए बीहड़ लड़ाई थी।
भाई कोहली जी ने मुझे अगले दिन अपने यहां भोजन करने और रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित किया। मेरी यात्रा-भीरुता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी लाने और मुझे अपने आवास तक ले चलने का प्रस्ताव भी रखा। वास्तव में एक विशेष कारणवश उनके यहां जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पड़ोसी और मित्र पंडित रामचंद्र शर्मा जब दिल्ली गए थे तो मेरा पत्र लेकर वे कोहली जी से मिलने भी गए थे। गाजीपुर लौटने पर शर्मा जी ने उनके स्वागत सत्कार की अति प्रशंसा के साथ उनके नवनिर्मित मकान की कुछ असाधारणता का वर्णन किया था।
उस असाधारणता-वर्णन से मेरे मानस-पटल पर जो चित्र बनता था, वह बहुत कलात्मक, मौलिक और रंगमंचीय भव्यता को लिए हुए होने के साथ बहुत प्रशस्त विशाल रूप में उभरता था। कोहली जी के साथ उनके मकान पर जाने के बाद मुझे लगा, मेरे भीतर उभरा चित्र गलत नहीं था। मगर अपने मकान की उक्त विशेषता के बारे में पूछने पर कोहली जी कहते हैं, ‘नहीं ! असाधारण कुछ नहीं है। बैठक का एक भाग प्राय: दस फुट ऊंचा है, दूसरा बीस फुट ! इससे यह सुविधा होती है कि दो तल होने पर भी मकान एक ही इकाई का होता है। जब मकान बनाया तो बच्चे छोटे थे। इसलिए मकान को दो तलों में विभाजित करने का मन नहीं हुआ। बैठक में से ही सीढ़ी ऊपर जाती है। मन में लोभ आने पर भी, मकान का कोई खंड किराए पर नहीं दिया जा सकता।
उक्त दस फुट तल पर बैठ कर कोहली जी उन दिनों सृजन-कार्य किया करते थे। तब वे रामकथा-संबंधी उपन्यासों की श्रृंखला को पूर्ण कर महाभारत पर भिड़े थे। इस कथा को उन्होंने ‘महासमर’ नाम दिया था। सन् 1988 ई. में उसका प्रथम भाग ‘बंधन’ के नाम से पाठकों के सामने आया और इसमें भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। इसमें कथाकार ने रामकथा वाले जनवादी रंग से हट कर कथा को मनोवैज्ञानिक रंगों से सज्जित किया था। इस प्रकार आस्वाद धरातल के परिवर्तनजन्य शिल्प चमत्कार से पाठकों को बेहद आकर्षित किया था।
वे टेबल के सामने जिस कुर्सी पर बैठ कर लिखते थे, उसके पीछे दीवार पर गणेश जी का एक भव्य चित्र लगा था।...तो यह रहस्य है महाभारत जैसे जटिल विशाल महापुराण में प्रवेश कर सफलता प्राप्ति का ? सहायक गणेश जी यहां भी मौजूद हैं।
कोहली जी के परिवार के साथ भोजन करते समय मैंने उक्त तथ्य को रहस्योद्घाटन की भूमिका बांध कर प्रस्तुत किया, तो बहुत हंसी हुई मालूम हुआ, वहां जानबूझ कर गणेश जी को प्रतिष्ठित नहीं किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से लगाये गये कैलेंडर के साथ वे तो अनायास ही आ विराजे हैं।...मैं सोचता हूं, वर्तमान में अनायास होने वाली बहुत सारी बातें भी भविष्य के लिए गहरा अर्थ रखती हैं। रामकथा के अज्ञात प्रभाव से लेखक का अन्तस रूपांतरित होने वाला था। अगली कृति के अज्ञात अनुकूल सहायक गणेश जी अनायास ही पीठ पीछे विराजमान हो गए थे। और आगे ‘तोड़ो कारा तोड़ो’ को पूर्ण करते-करते तो ऐसा लगता है कि लेखक में पूर्णत: रूपांतर घटित हो गया है।
ज्ञात हुआ है कि जिस कक्ष में बैठ कर वे नित्य आठ घंटे अपने को सृजन-यज्ञ में खपाया करते हैं, उसमें गणेश जी के अतिरिक्त हनुमान जी भी विराजित हैं। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की एक साढ़े चार फुट की मनोरम प्रतिमा है। राम जी भी हैं। प्रतीक्षा प्रभु इच्छा की है, एक पृथक मंदिर भी बनाने की इच्छा है। यह सब क्या है ? राम और कृष्ण-कथा के इस ईश्वरवाद रहित जनवादी लेखक के क्रमिक परिवर्तन को कृतियों के माध्यम से मैंने ध्यानपूर्वक देखा है।
‘अभिज्ञान’ (सन् 1981 ई.) में कोहली जी ने कृष्ण का मानवीकरण किया। कृष्ण और सुदामा की इस कहानी में सुदामा जी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास नहीं, राजनीतिक-सामाजिक चेतनासंपन्न जननेता कृष्ण के पास जाते हैं। ये कृष्ण भगवान नहीं, मधुर नास्तिक हैं। यहां अध्यात्म, राजनीति की शरण में जाता चित्रित है। कृष्ण ईश्वरावतार नहीं हैं । सुदामा की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक लिखता है। ‘‘वह इस प्रकार बातें करता है, जैसे वह स्वयं ही ईश्वर है।’’ लेखक कृष्ण के समस्त दैवी चमत्कारों को भौतिक या मानवीय चमत्कारों का रूप देकर प्रस्तुत करता है।
इससे पूर्व रामकथा को विस्तार से उठा कर इसमें भी पौराणिक मूल्य मान्यताओं की आधुनिक व्याख्या कर विचार-क्रान्ति का सूत्रपात किया गया था। ‘दीक्षा’, ‘अवसर’, ‘संघर्ष की ओर’ और ‘युद्ध’ नामक रामकथा श्रृंखला की कृतियों में कथाकार द्वारा सहस्राब्दियों की परंपरा से जनमानस में जमे ईश्वरावतार भाव और भक्तिभाव की जमीन को, उससे जुड़ी धर्म और ईश्वरवाची सांस्कृतिक जमीन को तोड़ा गया है। रामकथा की नई जमीन को नए मानवीय, विश्वसनीय, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ आधुनिक जनवादी अथवा भौतिक दृष्टि का चरमोत्कर्ष है। इसके बाद क्रमिक रूप से इसमें रूपांतर होता है, कुछ ‘महासमर’ में और बहुत कुछ भरपूर रूप में ‘तोड़ो कारा तोड़ो’ में। यह रूपांतरण लेखन-कक्ष में भी घटित होता है।
एक प्रश्न के उत्तर में कोहली जी कहते हैं, ‘‘जनवादी होने का अर्थ जड़वादी होना नहीं होता। मैं अभी भी जनवादी हूं, पर मार्क्सवादी नहीं हूं। जो जन-जन में ईश्वर को देखे, जनवादी तो वही है।’’ निस्संदेह यह जनवाद का एक नया मौलिक अर्थ है। सार्थक और समीचीन भी है। परंतु इस परंपरा से जुड़े हुए इस ईश्वरवादी अर्थ को आधुनिक जनवादी जन नहीं मानेंगे। उनका अर्थ फैशन की भांति फैला एक विशेष अर्थ है, जिसे अनेक लोग साहित्यिक फैशन की भांति ही ओढ़े हुए होते हैं। संभव है कोहली जी ने उक्त अर्थ को उस आधुनिक फैशन के चक्कर में ही कभी ओढ़ रखा हो, जो अब पूरी तरह उतार दिया गया है। अब वे पूर्णत: अपने सहज रूप में सृजन-संसार में खड़े हैं। वे खुल कर स्वीकार करते हैं :
‘‘प्रभु की कृपा है। उनसे प्रतिदिन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगता हूं। देखें, वे कब अपनी माया का निराकरण करते हैं। ‘विनय पत्रिका’ पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि मन में अभी सारे दुर्गुण विद्यमान है। जाने स्वच्छता कब आएगी। अपने लेखन के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।’’
‘लिखने का अर्थ’ शीर्षक अपने एक लंबे निबंध में कथाकार ने अपने व्यक्तिगत जीवन के भयानक संकट और उससे उबरने के माध्यम के रूप में ईश्वरवादी सृजन-सृष्टि के अनायास प्रादुर्भाव की स्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। संकट अनाम अनिष्ट की आशंका का रहा, जिसने उन्हें चिड़चिड़ा बना कर उखाड़ दिया था। गहरी अवसादग्रस्त स्थिति में उन्हें लगता कि उन्हें कोई अज्ञात बड़ा रोग हो गया है। इधर डॉक्टरों की दृष्टि में कोई शारीरिक रोग नहीं था। रोग मनोवैज्ञानिक था। घबराहट और हताशा बढ़ती ही जा रही थी।
उक्त स्थिति सन् 1964 ई.से लेकर निजी नए मकान में आने (सन् 1983) तक कम अधिक होती चली। इन्हीं दिनों ‘महासमर’ का लेखन चल रहा था। मन में इच्छा जगी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की और इसी संदर्भ में श्रीरामकृष्ण परमहंस को भी पढ़ा तो मन की कोई गांठ खुल गई उसके पश्चात् घटनाक्रम इस प्रकार घटित होने लगा कि कोहली जी के जीवन में और फिर लेखन में कृष्ण भगवान आ गए। उक्त लेख का अंत करते हुए, लेखक ने दो टूक शब्दों में अपने नए आस्थावादी अनुभव का वर्णन किया है :
‘‘...पूजा करने के लिए श्रीकृष्ण के सम्मुख बैठा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। आज मेरी समझ में आ रहा था, हमारा सारा अहंकार मिथ्या था।..मेरा सारा पराक्रम शांत हो चुका था। मैं पूर्णत: असहाय हो गया था तो उसने स्वयं ही संदेश भेजा था।।.. जब हम अपनी क्षमताओं के अहंकार को भुलाकर उसकी शक्ति पर आश्रित होते हैं, तो कैसे वह चुटकी बजाते ही सारे काम कर देता है।
‘....ईश्वर मेरे सम्मुख उपस्थित नहीं था, किंतु मेरे चारों ओर वर्तमान था। मैं उसे देख नहीं सकता था, परंतु उसे अनुभव कर सकता था।...मेरे लेखन में अकस्मात् कृष्ण चले आए थे। कथानक अथवा कथ्य के तर्क पर मैं उनका महत्त्व कम नहीं कर सकता था। मैं उनको बहिष्कृत नहीं कर सकता था। स्वयं को ही उनके रंग में अधिक-से-अधिक रंग सकता था।
‘‘सौभाग्य तो था इस स्कूल के पीछे प्रच्छन्न उस सूक्ष्म से परिचय। ऐश्वर्य को पार कर ईश्वर से परिचय। अब समझ में आया था कि मैं अपने साहित्य से क्या प्राप्त कर रहा हूं। अपने इस विकास के माध्यम का महत्त्व ही मेरे लिए कुछ अधिक हो गया था।’’
मेरी दृष्टि में ऐसा होना स्वाभाविक ही था। भले ही आरंभ में राम और कृष्ण में परंपरागत ईश्वरत्व, अवतार भाव और अतिमानवीय देवत्व को आधुनिक अर्थ दिया गया, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि कथाकार नरेन्द्र कोहली ने उपन्यस्त करने के लिए सुदीर्घ काल तक मनोयोग से उनके चरित्र और लीला प्रकरण का अवगाहन किया। दूसरे सटीक शब्दों में उनका भजन किया, नामजप किया। भजन का प्रभाव होना ही था। तुलसी ने लिखा है :
‘साथ सहा गया दुख’ (सन् 1974 ई.) पर भी मैंने लिखा। यह देख कर मुझे आश्चर्य होता था कि मात्र ढाई पात्रों (पति, पत्नी और एक नवजात बच्ची) का सादा सपाट घरेलू या पारिवारिक उपन्यास इतना आकर्षक और गतिवान कैसे बन गया है। अनलंकृत जीवन-भाषा में सादगी का सौंदर्य घोल कर किस कला से इसे इतनी सघन संवेदनीयता से पूर्ण बनाया गया है। बाद में मालूम हुआ कि पहली बच्ची के जन्म और मृत्यु की यह जो कथा सन् 1966-67 ई. में लिखी गई, उसमें कल्पना बहुत कम है। जो है, वह लेखक का अनुभव है, भोगा हुआ सत्य है। इतने पर भी उस भुक्त दु:ख-सत्य को पारिवारिक जीवन-मूल्यों के शिव से संपृक्त कर, रचनात्मक स्तर पर प्रस्तुत कर देने वाले शिल्प-सौंदर्य का सवाल तो लेखक की ओर आकर्षित कर ही देता है।
यह आकर्षण सन् 1975 ई. से और अधिक बढ़ गया। उनकी रामकथा वाली श्रृंखला की पहली कृति ‘दीक्षा’ इसी समय छपी थी। इसमें परंपरित अवधारणाओं पर जो नई प्रगतिशील जनवादी कलम लगाई गई थी, उसने कृति को जोरदार चर्चा का विषय बना दिया। एक प्रश्न उठा कि श्रद्धा, भावुकता और पूज्य-भाव की अतिमानवीय कल्पनाओं को बुद्धिवादी कैंची से कतर डालना और पौराणिक अथवा सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक राजनीतिक व्याख्या प्रस्तुत करना कहां तक उचित है ? इसका उत्तर नरेन्द्र कोहली ने ‘दीक्षा’ की भूमिका में देने का प्रयत्न किया है। बांगलादेश में क्रूर पाकिस्तानी सेनाओं के बर्बर अत्याचार और बुद्धिजीवियों के व्यापक संहार को देख कर उपन्यासकार के मन में रामकथा की नई व्याख्या उभर आती है और वह सोचता है, ‘‘बांगलादेश कहां है ? वह सिद्धाश्रम में भी हो सकता है।...पाकिस्तान तब नहीं था, किंतु राक्षस तो थे।...’’ इस प्रकार विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में तत्कालीन बुद्धिजीवियों की पीड़ाप्रसूत, राम के क्रांतिकारी नेतृत्व की यह नूतन गाथा उपन्यस्त होती है।
‘दीक्षा’ के बाद अगले वर्ष सन् 1976 ई. में रामकथा का दूसरा भाग ‘अवसर’ और इसी प्रकार प्रतिवर्ष उस श्रृंखला के एक-एक नए भाग के प्रकाशन-क्रम में सन् 1979 ई. तक शेष ‘संघर्ष की ओर’ और ‘युद्ध’ (दो भाग) का प्रकाशन संपन्न हो गया। वास्तव में यह बहुत श्रमसाध्य और महान् कार्य रहा। इसकी संपन्नता के साथ लेखक के रचनात्मक व्यक्तित्व की ऊंचाई बहुत बढ़ गई। ऐसे प्रिय लेखक से मिलना एक सुखद अनुभव था। मिलने का यह पहला मौका कलकत्ते में भारतीय संस्कृति संसद की ओर से आयोजित सन् 1983 ई. वाले कथा-समारोह में मिला। यह आयोजन 23 दिसंबर से शुरू होकर तीन दिनों तक रहा। इस में जैनेंद्र जी, निर्मल वर्मा, रामदरश मिश्र, भीष्म साहनी, अवध नारायण मुद्गल, राजी सेठ, उषा प्रियंवदा, गोविन्द मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, हिमांशु जोशी, बटरोही, सिद्धेश, प्रभाकर माचवे, चंद्रकांत बांदिवडेकर और नरेन्द्र कोहली आदि लेखकों ने भाग लिया था।
नरेन्द्र कोहली को इस समारोह में निकट से देखने का मौका मिला। वे कम बोलने वाले, गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति लगे। अपने भाषणों में वे समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से उठाते रहे। वे अपने को प्रस्तुत करने में बहुत सावधानी बरतते रहे। वे कभी बलपूर्वक स्थापित करने की चेष्टा नहीं करते थे। उनके विचारों में विस्तार-वृत्ति होती थी। इतने पर भी वे बोलने में अधिक समय नहीं लेते थे। उनका बोलना मौलिक चिंतन और आधुनिकता की चेतना से पूर्ण होता। उक्त सम्मेलन में अंतिम दिन 25 दिसंबर को अंतिम सत्र ‘मूल्य : मूल्यांकन : पुनर्मूल्यांकन’ के अंतर्गत डॉ.नरेन्द्र कोहली ने कहा, ‘‘जिस रचनाकार के पास कहने को अपनी बात है, वही काल-प्रवाह में टिक पाता है। यही कारण है कि प्रेमचंद का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, जबकि उग्र, चतुरसेन शास्त्री आदि अपने समय में बहुत चर्चित होने के बावजूद आज धूमिल होते जा रहे हैं।’’
उक्त कथन में ‘अपनी बात’ वाला तथ्य बहुत मूल्यवान है। नए बदलते समाज की नई चेतना और नई संवेदना तथा नई सोच को, ताजी ऊर्जा के साथ मौलिक शिल्प में प्रस्तुत करने वाले कथाकार नरेन्द्र कोहली के पास निर्विवाद रूप से कहने के लिए अपनी बात है। यहां तक कि वे वाल्मीकि और व्यास की बातों को उठाते हैं तो उसे प्रस्तुत करने में अपनी बात बना देते हैं और अविरोध, अनवरोध कह डालते हैं। अपने इसी नवाग्रही व्यक्तित्व के चलते ही वे अत्यंत जागरूकता के साथ जहां भी अवसर मिलता है, नएपन को अन्वेषित करते रहते हैं।
कलकत्ते के उक्त कथा-समारोह में यद्यपि पूरे दिन के कार्यक्रम बहुत कसावपूर्ण होते थे, तथापि रात में समय निकाल कर कोहली जी कलकत्ते की रंगकर्मी संस्थाओं को आधुनिकतम प्रस्तुतियों को बहुत रुचिपूर्वक देख आते थे। इस कार्य में मार्गदर्शक श्री विष्णुकांत शास्त्री हुआ करते थे। कलकत्ते के प्रयोगधर्मी नाटकों, उनको प्रस्तुत करने वाली विविध संस्थाओं, रंगमंचों तथा रंगशिल्पियों आदि में शास्त्री जी की बहुत गहरी पैठ थी। वे स्वयं उनके अटूट भाव से जुड़े थे और उनकी ओर से वे आगत कथाकारों को विधिवत् आमंत्रित करते थे। लोग जाते भी थे और रंगमंचविहीन तथा रंगसज्जा आदि रहित अनौपचारिक प्रस्तुतियों से प्रभावित भी होते थे। स्वयं आधुनिक दृष्टिसंपन्न कथाकार के साथ नाटककार होने के कारण नरेन्द्र कोहली इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। ‘शंबूक की हत्या’ निर्णय रुका हुआ, और ‘गारे की दीवार’—तीन नाट्य कृतियां, तब तक प्रकाशित हो चुकी थीं और किसी-न-किसी कोने से चर्चा आ जाती थीं।
दूसरी बार कुछ और अधिक निकट से परिचय का सुयोग एक स्वागत समारोह में हुआ। स्वागत मेरा ही हो रहा था। समारोह अखिल भारतीय लेखक संगठन, दिल्ली की ओर से डॉ.रामदरश मिश्र ने अपने आवास पर (17 फरवरी सन् 1987 ई.) आयोजित किया गया था। मैं उन दिनों उनका अतिथि था। पहली बार दिल्ली गया था। मेरा गंवार लेखक इस स्वागत से बहुत संकुचित हो रहा था। समारोह में कोहली जी के अतिरिक्त डॉ.कमलकिशोर गोयनका, डॉ.नरेन्द्र मोहन, डॉ.रमाकांत श्रीवास्तव, डॉ.ललित शुक्ल, डॉ.विजयेन्द्र स्नातक, और डॉ.विनय आदि साहित्यकार उपस्थित थे। डॉ.नरेन्द्र कोहली ने दिल्ली-संबंधी मेरे अनुभव के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उसे एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, ‘‘दिल्ली एक लड़ाई है।’’ और फिर अपनी यात्रा-भीरुता के परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या की। सचमुच डॉ.मिश्र के साथ दिल्ली में लगभग एक सप्ताह तक घूमने में मुझे ऐसा ही लगा था। कहीं भी जाना, बसों की भारी भीड़ में धंसना मेरे लिए बीहड़ लड़ाई थी।
भाई कोहली जी ने मुझे अगले दिन अपने यहां भोजन करने और रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित किया। मेरी यात्रा-भीरुता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी लाने और मुझे अपने आवास तक ले चलने का प्रस्ताव भी रखा। वास्तव में एक विशेष कारणवश उनके यहां जाने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पड़ोसी और मित्र पंडित रामचंद्र शर्मा जब दिल्ली गए थे तो मेरा पत्र लेकर वे कोहली जी से मिलने भी गए थे। गाजीपुर लौटने पर शर्मा जी ने उनके स्वागत सत्कार की अति प्रशंसा के साथ उनके नवनिर्मित मकान की कुछ असाधारणता का वर्णन किया था।
उस असाधारणता-वर्णन से मेरे मानस-पटल पर जो चित्र बनता था, वह बहुत कलात्मक, मौलिक और रंगमंचीय भव्यता को लिए हुए होने के साथ बहुत प्रशस्त विशाल रूप में उभरता था। कोहली जी के साथ उनके मकान पर जाने के बाद मुझे लगा, मेरे भीतर उभरा चित्र गलत नहीं था। मगर अपने मकान की उक्त विशेषता के बारे में पूछने पर कोहली जी कहते हैं, ‘नहीं ! असाधारण कुछ नहीं है। बैठक का एक भाग प्राय: दस फुट ऊंचा है, दूसरा बीस फुट ! इससे यह सुविधा होती है कि दो तल होने पर भी मकान एक ही इकाई का होता है। जब मकान बनाया तो बच्चे छोटे थे। इसलिए मकान को दो तलों में विभाजित करने का मन नहीं हुआ। बैठक में से ही सीढ़ी ऊपर जाती है। मन में लोभ आने पर भी, मकान का कोई खंड किराए पर नहीं दिया जा सकता।
उक्त दस फुट तल पर बैठ कर कोहली जी उन दिनों सृजन-कार्य किया करते थे। तब वे रामकथा-संबंधी उपन्यासों की श्रृंखला को पूर्ण कर महाभारत पर भिड़े थे। इस कथा को उन्होंने ‘महासमर’ नाम दिया था। सन् 1988 ई. में उसका प्रथम भाग ‘बंधन’ के नाम से पाठकों के सामने आया और इसमें भी उन्हें भरपूर ख्याति मिली। इसमें कथाकार ने रामकथा वाले जनवादी रंग से हट कर कथा को मनोवैज्ञानिक रंगों से सज्जित किया था। इस प्रकार आस्वाद धरातल के परिवर्तनजन्य शिल्प चमत्कार से पाठकों को बेहद आकर्षित किया था।
वे टेबल के सामने जिस कुर्सी पर बैठ कर लिखते थे, उसके पीछे दीवार पर गणेश जी का एक भव्य चित्र लगा था।...तो यह रहस्य है महाभारत जैसे जटिल विशाल महापुराण में प्रवेश कर सफलता प्राप्ति का ? सहायक गणेश जी यहां भी मौजूद हैं।
कोहली जी के परिवार के साथ भोजन करते समय मैंने उक्त तथ्य को रहस्योद्घाटन की भूमिका बांध कर प्रस्तुत किया, तो बहुत हंसी हुई मालूम हुआ, वहां जानबूझ कर गणेश जी को प्रतिष्ठित नहीं किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से लगाये गये कैलेंडर के साथ वे तो अनायास ही आ विराजे हैं।...मैं सोचता हूं, वर्तमान में अनायास होने वाली बहुत सारी बातें भी भविष्य के लिए गहरा अर्थ रखती हैं। रामकथा के अज्ञात प्रभाव से लेखक का अन्तस रूपांतरित होने वाला था। अगली कृति के अज्ञात अनुकूल सहायक गणेश जी अनायास ही पीठ पीछे विराजमान हो गए थे। और आगे ‘तोड़ो कारा तोड़ो’ को पूर्ण करते-करते तो ऐसा लगता है कि लेखक में पूर्णत: रूपांतर घटित हो गया है।
ज्ञात हुआ है कि जिस कक्ष में बैठ कर वे नित्य आठ घंटे अपने को सृजन-यज्ञ में खपाया करते हैं, उसमें गणेश जी के अतिरिक्त हनुमान जी भी विराजित हैं। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की एक साढ़े चार फुट की मनोरम प्रतिमा है। राम जी भी हैं। प्रतीक्षा प्रभु इच्छा की है, एक पृथक मंदिर भी बनाने की इच्छा है। यह सब क्या है ? राम और कृष्ण-कथा के इस ईश्वरवाद रहित जनवादी लेखक के क्रमिक परिवर्तन को कृतियों के माध्यम से मैंने ध्यानपूर्वक देखा है।
‘अभिज्ञान’ (सन् 1981 ई.) में कोहली जी ने कृष्ण का मानवीकरण किया। कृष्ण और सुदामा की इस कहानी में सुदामा जी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास नहीं, राजनीतिक-सामाजिक चेतनासंपन्न जननेता कृष्ण के पास जाते हैं। ये कृष्ण भगवान नहीं, मधुर नास्तिक हैं। यहां अध्यात्म, राजनीति की शरण में जाता चित्रित है। कृष्ण ईश्वरावतार नहीं हैं । सुदामा की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक लिखता है। ‘‘वह इस प्रकार बातें करता है, जैसे वह स्वयं ही ईश्वर है।’’ लेखक कृष्ण के समस्त दैवी चमत्कारों को भौतिक या मानवीय चमत्कारों का रूप देकर प्रस्तुत करता है।
इससे पूर्व रामकथा को विस्तार से उठा कर इसमें भी पौराणिक मूल्य मान्यताओं की आधुनिक व्याख्या कर विचार-क्रान्ति का सूत्रपात किया गया था। ‘दीक्षा’, ‘अवसर’, ‘संघर्ष की ओर’ और ‘युद्ध’ नामक रामकथा श्रृंखला की कृतियों में कथाकार द्वारा सहस्राब्दियों की परंपरा से जनमानस में जमे ईश्वरावतार भाव और भक्तिभाव की जमीन को, उससे जुड़ी धर्म और ईश्वरवाची सांस्कृतिक जमीन को तोड़ा गया है। रामकथा की नई जमीन को नए मानवीय, विश्वसनीय, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ आधुनिक जनवादी अथवा भौतिक दृष्टि का चरमोत्कर्ष है। इसके बाद क्रमिक रूप से इसमें रूपांतर होता है, कुछ ‘महासमर’ में और बहुत कुछ भरपूर रूप में ‘तोड़ो कारा तोड़ो’ में। यह रूपांतरण लेखन-कक्ष में भी घटित होता है।
एक प्रश्न के उत्तर में कोहली जी कहते हैं, ‘‘जनवादी होने का अर्थ जड़वादी होना नहीं होता। मैं अभी भी जनवादी हूं, पर मार्क्सवादी नहीं हूं। जो जन-जन में ईश्वर को देखे, जनवादी तो वही है।’’ निस्संदेह यह जनवाद का एक नया मौलिक अर्थ है। सार्थक और समीचीन भी है। परंतु इस परंपरा से जुड़े हुए इस ईश्वरवादी अर्थ को आधुनिक जनवादी जन नहीं मानेंगे। उनका अर्थ फैशन की भांति फैला एक विशेष अर्थ है, जिसे अनेक लोग साहित्यिक फैशन की भांति ही ओढ़े हुए होते हैं। संभव है कोहली जी ने उक्त अर्थ को उस आधुनिक फैशन के चक्कर में ही कभी ओढ़ रखा हो, जो अब पूरी तरह उतार दिया गया है। अब वे पूर्णत: अपने सहज रूप में सृजन-संसार में खड़े हैं। वे खुल कर स्वीकार करते हैं :
‘‘प्रभु की कृपा है। उनसे प्रतिदिन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगता हूं। देखें, वे कब अपनी माया का निराकरण करते हैं। ‘विनय पत्रिका’ पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि मन में अभी सारे दुर्गुण विद्यमान है। जाने स्वच्छता कब आएगी। अपने लेखन के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।’’
‘लिखने का अर्थ’ शीर्षक अपने एक लंबे निबंध में कथाकार ने अपने व्यक्तिगत जीवन के भयानक संकट और उससे उबरने के माध्यम के रूप में ईश्वरवादी सृजन-सृष्टि के अनायास प्रादुर्भाव की स्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। संकट अनाम अनिष्ट की आशंका का रहा, जिसने उन्हें चिड़चिड़ा बना कर उखाड़ दिया था। गहरी अवसादग्रस्त स्थिति में उन्हें लगता कि उन्हें कोई अज्ञात बड़ा रोग हो गया है। इधर डॉक्टरों की दृष्टि में कोई शारीरिक रोग नहीं था। रोग मनोवैज्ञानिक था। घबराहट और हताशा बढ़ती ही जा रही थी।
उक्त स्थिति सन् 1964 ई.से लेकर निजी नए मकान में आने (सन् 1983) तक कम अधिक होती चली। इन्हीं दिनों ‘महासमर’ का लेखन चल रहा था। मन में इच्छा जगी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की और इसी संदर्भ में श्रीरामकृष्ण परमहंस को भी पढ़ा तो मन की कोई गांठ खुल गई उसके पश्चात् घटनाक्रम इस प्रकार घटित होने लगा कि कोहली जी के जीवन में और फिर लेखन में कृष्ण भगवान आ गए। उक्त लेख का अंत करते हुए, लेखक ने दो टूक शब्दों में अपने नए आस्थावादी अनुभव का वर्णन किया है :
‘‘...पूजा करने के लिए श्रीकृष्ण के सम्मुख बैठा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। आज मेरी समझ में आ रहा था, हमारा सारा अहंकार मिथ्या था।..मेरा सारा पराक्रम शांत हो चुका था। मैं पूर्णत: असहाय हो गया था तो उसने स्वयं ही संदेश भेजा था।।.. जब हम अपनी क्षमताओं के अहंकार को भुलाकर उसकी शक्ति पर आश्रित होते हैं, तो कैसे वह चुटकी बजाते ही सारे काम कर देता है।
‘....ईश्वर मेरे सम्मुख उपस्थित नहीं था, किंतु मेरे चारों ओर वर्तमान था। मैं उसे देख नहीं सकता था, परंतु उसे अनुभव कर सकता था।...मेरे लेखन में अकस्मात् कृष्ण चले आए थे। कथानक अथवा कथ्य के तर्क पर मैं उनका महत्त्व कम नहीं कर सकता था। मैं उनको बहिष्कृत नहीं कर सकता था। स्वयं को ही उनके रंग में अधिक-से-अधिक रंग सकता था।
‘‘सौभाग्य तो था इस स्कूल के पीछे प्रच्छन्न उस सूक्ष्म से परिचय। ऐश्वर्य को पार कर ईश्वर से परिचय। अब समझ में आया था कि मैं अपने साहित्य से क्या प्राप्त कर रहा हूं। अपने इस विकास के माध्यम का महत्त्व ही मेरे लिए कुछ अधिक हो गया था।’’
मेरी दृष्टि में ऐसा होना स्वाभाविक ही था। भले ही आरंभ में राम और कृष्ण में परंपरागत ईश्वरत्व, अवतार भाव और अतिमानवीय देवत्व को आधुनिक अर्थ दिया गया, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि कथाकार नरेन्द्र कोहली ने उपन्यस्त करने के लिए सुदीर्घ काल तक मनोयोग से उनके चरित्र और लीला प्रकरण का अवगाहन किया। दूसरे सटीक शब्दों में उनका भजन किया, नामजप किया। भजन का प्रभाव होना ही था। तुलसी ने लिखा है :
भाव कुभाव अनख आलसहू।
नाम तपत मंगल दिसि दसहू।।
नाम तपत मंगल दिसि दसहू।।
उक्त मंगल को लेखक के संदर्भ में सृजन-मंगल के रूप में मैंने देखा है।
उनकी कृति ‘तोड़ो कारा तोड़ो’ (सन् 1992-93 ई.) को
मैंने अपने एक निबंध में अध्यात्मवाद के राष्ट्रीय गढ़ और मनोमय सक्रिय
आध्यात्मिक सत्संग के रूप में विश्लेषित किया है। इस कृति को पढ़ कर मुझे
बारंबार ऐसा लगता है कि दोनों नरेन्द्र (स्वामी विवेकानंद का भी पूर्व नाम
नरेन्द्र ही था) में बदलाव की स्थिति एक-सी है। यथार्थवादी और ईश्वर के
प्रति शंकाशील बंग युवक नरेन्द्रनाथ दत्त के श्रीरामकृष्ण परमहंस की साधना
के ताप से पिघलने की घटना को चित्रांकित करने वाला सिद्ध हिंदी कथाकार भी
पिघल कर ही लेखनी उठाता है। यही कारण है कि कृति में इतना जबर्दस्त प्रभाव
आ गया है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i